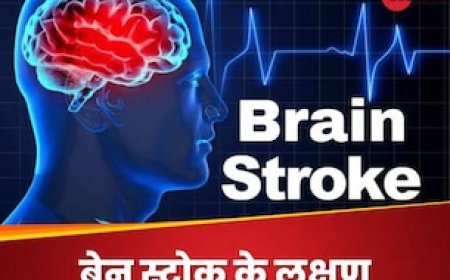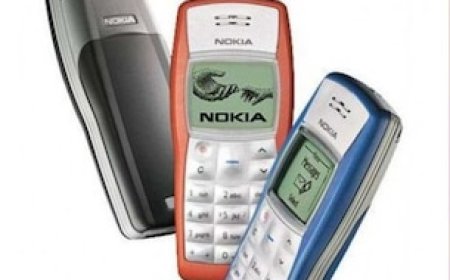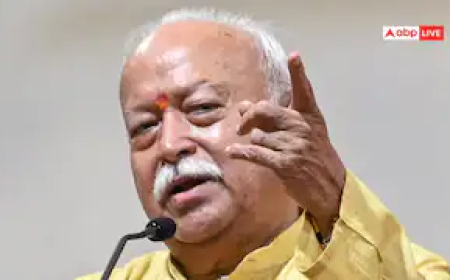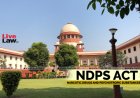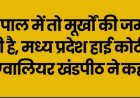महिला वकीलों की सुरक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल्स को POSH Act के तहत लाने पर केंद्र और BCI को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सुरक्षा उन महिला अधिवक्ताओं को दी जाए जो राज्य बार काउंसिल के साथ पंजीकृत हैं और अदालतों के समक्ष अभ्यास कर रही हैं। याचिका में बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को महिला अधिवक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए आंतरिक समितियों का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
"पॉश अधिनियम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा और अनुच्छेद 19 (1) (g) के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता के लिए एक महिला के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिसमें यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार शामिल है। क़ानून का उद्देश्य और डिजाइन इन अधिकारों को प्रभावी करना है, और कोई भी व्याख्या जो महिला अधिवक्ताओं को इसके संरक्षण से बाहर करती है, उस संवैधानिक उद्देश्य के विपरीत है जिसे अधिनियम पूरा करना चाहता है।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने 'ब्रेकिंग द साइलेंस: ए हैंडबुक ऑन द पॉश एक्ट' की लेखिका और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) की आंतरिक समिति की सदस्य अधिवक्ता सीमा जोशी द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। याचिका में UNS महिला कानूनी संघ (पंजीकृत) बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य में बॉम्बे हाईकोर्ट के 7 जुलाई, 2025 के फैसले को रद्द करने का भी प्रयास किया गया है। इस हद तक कि यह पॉश अधिनियम को बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के कर्मचारियों तक सीमित रखता है।
याचिका में कहा गया है कि फैसले में गलत तरीके से महिला अधिवक्ताओं को प्रतिबंधात्मक व्याख्या अपनाकर अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। याचिका में दलील दी गई है कि पॉश अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर मौजूद 'किसी भी महिला' को कवर करना है, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं। अंतरिम राहत के रूप में, याचिका में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और बार काउंसिलों, बार एसोसिएशनों और इसी तरह के संस्थानों द्वारा गठित सभी आंतरिक समितियों को महिला अधिवक्ताओं द्वारा शिकायतों पर सुनवाई जारी रखने का अनुरोध किया गया है। जस्टिस नागरत्ना ने आज सुनवाई के दौरान सवाल किया कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दायर की जा सकती है। खंडपीठ ने कहा, ''या तो आप अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर करें या बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को एसएलपी के रूप में चुनौती दें। आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो इसे ठीक से करें", जवाब में, याचिकाकर्ता की वकील रितिका वोहरा ने हाईकोर्ट के फैसले और रोक के लिए अंतरिम प्रार्थना को रद्द करने की मांग करने वाली प्रार्थना पर जोर नहीं देने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल और महाराष्ट्र राज्य को प्रतिवादी के रूप में हटाने पर भी सहमति व्यक्त की। याचिका में अधिनियम की धारा 2 (a) का हवाला दिया गया है, जो एक "पीड़ित महिला" को "चाहे वह कार्यरत हो या नहीं" के रूप में परिभाषित करती है, और धारा 3, जो कार्यस्थल पर "किसी भी महिला" के खिलाफ यौन उत्पीड़न को प्रतिबंधित करती है। याचिका में धारा 2 (o) (i) पर भरोसा किया गया है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अदालतें, बार काउंसिल कार्यालय और बार एसोसिएशन "संस्थान" या "प्रतिष्ठान" हैं और अधिनियम के भीतर "कार्यस्थल" के दायरे में आते हैं। यह तर्क देता है कि बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वैधानिक निकाय हैं, और बार एसोसिएशन राज्य के बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित अदालत परिसर के भीतर काम करते हैं; इसलिए, धारा 4 के तहत, प्रत्येक को महिला अधिवक्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम एक आंतरिक समिति का गठन करना चाहिए।
यह आगे मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी निर्देशों की ओर इशारा करता है, जहां बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों को महिला अधिवक्ताओं से यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए निवारण तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। याचिका में दावा किया गया है कि इन निर्देशों पर विचार करने में विफल रहने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अनुचित है। "हाईकोर्ट के दिनांक 7.7.2025 के निर्णय में महिला पेशेवरों के एक पूरे वर्ग को बाहर करने का तत्काल और हानिकारक प्रभाव है - अर्थात्, महिला अधिवक्ताओं - को POSH अधिनियम द्वारा परिकल्पित वैधानिक संरक्षण और निवारण तंत्र से, क़ानून की सरल भाषा के बावजूद, इसकी विस्तृत परिभाषाएँ, मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ (2013) 1 SCC 297, और अदालतों, बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को पीओएसएच अधिनियम के अर्थ के भीतर 'कार्यस्थल' के रूप में मानने की लगातार संस्थागत प्रथा", याचिका में कहा गया है। याचिका में महिला अधिवक्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पहले से गठित आंतरिक समितियों, दिल्ली उच्च न्यायालय के ढांचे को मान्यता दी गई है कि अदालत की सेटिंग में शिकायतकर्ताओं और उत्तरदाताओं में वकील और वादी शामिल हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 2013 के नियमों को "किसी भी महिला सुप्रीम कोर्ट परिसर में किसी भी आयु का, चाहे वह नियोजित हो या न हो। यह तर्क देता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय इस संस्थागत प्रथा को कमजोर करता है और एक वैधानिक शून्य बनाता है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग महिला अधिवक्ताओं के लिए पॉश के उद्देश्यपूर्ण आवेदन को सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए।
साभार